डीजे के शोर में लुप्त हो रही झारखंड की लोकधुन, जानिए जंग लड़ता तुरी समाज की मिसाल की मिसाल
देवघर: कभी झारखंड की सुबह ढोल और नागाडो की गूंज से होती थी. यह सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि गांव की पहचान, परंपरा और सामूहिक खुशियों की आवाज होती थी। विवाह-ब्याह, नामकरण, पर्व-त्योहार या कोई भी सामाजिक संस्कार तुरी समाज के बिना हर आयोजन को अधूरा माना जाता था। ढोल की हर थाप में उत्सव की उमंग और नागाडो की गूंज में पूरे गांव की खुशियां समा जाती थी। लेकिन समय के साथ लोगों की पसंद बदली और उसी के साथ तुरी समाज का जीवन भी बदल गया। आधुनिकता की चमक और डीजे की तेज़ आवाज़ ने उस लोकधुन को पीछे छोड़ दिया, जिसे कभी मादक की आत्मा कहा गया था। आज वही ढोल-नगाड़े, जो कभी सम्मान और अपमान का साधन थे, अब घर के घरों में धूल फांकते नजर आते हैं।
तीस नहीं काम
झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला तुरी समाज आज गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भगवानपुर, चुल्हिया और आसपास के इलाकों में रोज़ रहने वाले सैकड़ों परिवारों की रोटी-रोटी समान पारंपरिक कला पर प्रतिबंध थी। पहले पूरे साल किसी न किसी कार्यक्रम में ढोल बजाने का काम मिलता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि महीनों तक कोई काम नहीं मिलता। ढोल वादक बसंत तुरी के साथी हैं कि पहली बार शादी-ब्याह के सीजन में ही घर-घर से बुलाया गया था। उसी कमाई से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और त्योहार पूरा होता था। अब लोग डीजे बजाकर खुशियां सिखाते हैं। हमारा थाप सुनने का वक्ता किसी के पास नहीं है। कई बार हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि दो स्पीकर की रोटियां बनाना भी मुश्किल हो जाता है।
सरकारी कार्यक्रम में दिखाया गया, स्थायी सहारा नहीं
दूसरी बात यह है कि जब भी कोई बड़ा सरकारी या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री, मंत्री या बड़े अधिकारी झारखंड आते हैं, तब मंच की शान बढ़ाने के लिए तुरी समाज को बुलाया जाता है। ढोल-नगाड़ों की गूंज से झारखंड की संस्कृति का मंदिर है। कैमरे चलते हैं, तस्वीरें ख़ानदानी होती हैं और तालियाँ बजती हैं। लेकिन कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है और कलाकार फिर अपने संघर्ष से जीवन में लौट आते हैं। सम्मान तो है, लेकिन स्थायी रोजगार नहीं है और भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है।
शिक्षा और गरीबी की समस्याएँ
आर्थिक तंगी के साथ-साथ शिक्षा की कमी तुरी समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। समाज के बहुत कम लोग पढ़ते-लिखते हैं। अधिकांश परिवार सुदूरवर्ती और जंगली इलाक़ों में रहते हैं, जहाँ स्कूल, सड़क और अन्य भव्य वस्तुओं का अभाव है। गरीबी के कारण बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। जब पेट की चिंता होती है तो शिक्षा को सबसे पहले छूट मिलती है। शिक्षा की कमी के कारण तुरी समाज के लोग सरकारी मान्यता की सही जानकारी भी नहीं। कला और कलाकारी के लिए बनी कई आकृतियाँ कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं। इसका परिणाम यह है कि यह पुरातन परम्परा धीरे-धीरे बदलती जा रही है।
नई पीढ़ी अपनी परंपरा से दूर हो रही है
सबसे बड़ी चिंता अगली पीढ़ी लेकर आती है. आज तुरी समाज के युवा ढोल और नगाड़े को अपना भविष्य नहीं मानते। वे व्यवसायियों, शहरों में छोटे-मोटे काम या अन्य कारीगरों की ओर रुख कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इस कला में न तो स्थायी हिस्सेदारी है और न ही कोई सुरक्षा है। कई घरों में अब ढोल-नगाड़े बजाते नहीं, बल्कि सिर्फ यादों के रूप में रखे जाते हैं।
प्रशिक्षण और अवसर मिले तो बदल सकते हैं हालात
चुल्हिया बागानों के युवाओं का कहना है कि अगर सरकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण दे, तो चश्मे बदले जा सकते हैं। उन्हें मंच, सम्मान और नियमित रोजगार मिले, तो वे अपनी कला को शामिल नहीं करते। इससे न केवल उनका जीवन बेहतर होगा, बल्कि झारखंड की लोकसंस्कृति भी जीवित रहेगी।
तुरी समाज का साफ कहना है कि वे भीख नहीं, बल्कि अपनी भूख की पहचान और अवसर चाहते हैं। उनका आग्रह है कि सरकारी शिक्षा की व्यवस्था की जाये, प्रशिक्षण केन्द्र को बढ़ावा दिया जाये, नियमित कार्यक्रमों में उन्हें शामिल किया जाये और उनकी कला को रोजगार से जोड़ा जाये। अगर अब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब तक झारखंड की पहचान बनाने वाले ढोल-नगाड़ों की थाप सिर्फ गरीबों और मंचों तक ही सीमित रह जाएगी, और एक पूरा समाज इतिहास के अनुयायियों में खो जाएगा।

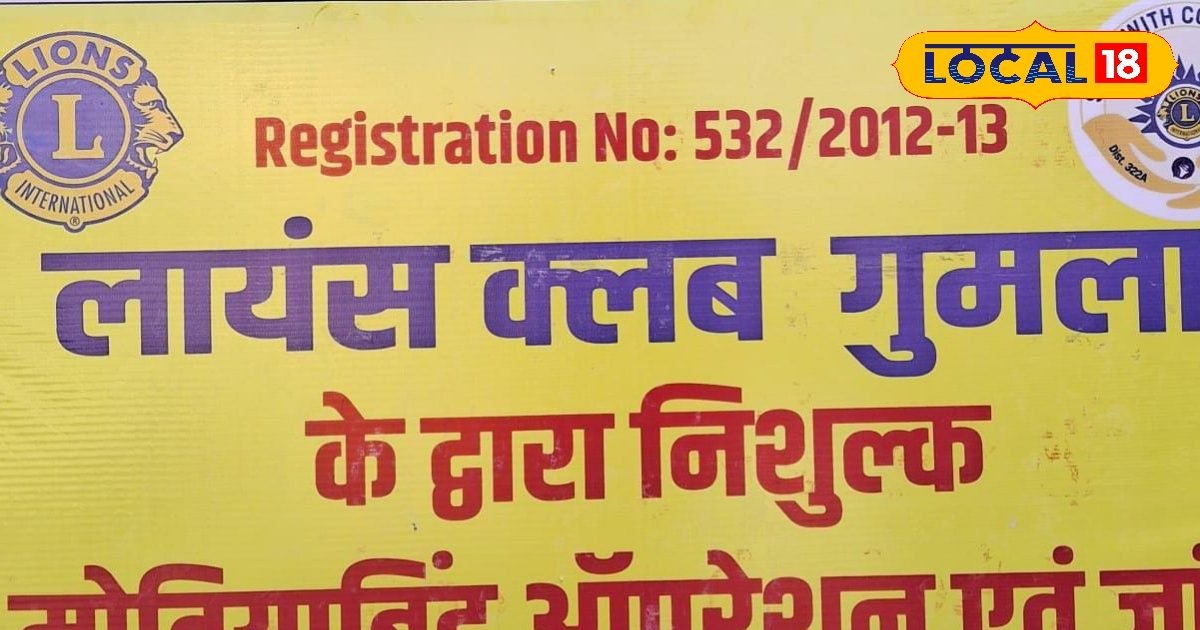











Post Comment